कोई साल बारिश का रूठ जाना तो कभी ज्यादा ही बरस जाना हमारे देश की नियति है। थोड़ा ज्यादा बरसात हो जाए तो उसके समेटने के साधन नहीं बचते और कम बरस जाए तो ऐसा रिजर्व स्टॉक नहीं दिखता जिससे काम चलाया जा सके।
अनुभवों से यह तो स्पष्ट है कि भारी-भरकम बजट, राहत, नलकूप जैसे शब्द जल संकट के निदान नहीं हैं। करोड़ों-अरबों की लागत से बने बांध सौ साल भी नहीं चलते, जबकि हमारे पारंपरिक ज्ञान से बनी जल संरचनाएं ढेर सारी उपेक्षा, बेपरवाही के बावजूद आज भी पानीदार हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरे के सामने आधुनिक इंजीनियरिंग बेबस है। यदि भारत का ग्रामीण जीवन और खेती बचाना है तो बारिश की हर बूंद को सहेजने के अलावा और कोई चारा नहीं बच रहा है।
देश के बहुत बड़े हिस्से के लिए अल्प वष्रा नई बात नहीं है, और न ही वहां के समाज के लिए कम पानी में गुजारा करना, लेकिन बीते पांच दशक के दौरान आधुनिकता की आंधी में दफन हो गए हजारों चंदेल-बुंदेला कालीन तालाबों और पारंपरिक जल पण्रालियों के चलते ये हालात बने। मप्र के बुरहानपुर शहर की आबादी तीन लाख के आसपास है। निमाड़ का यह इलाका पानी की कमी के लिए जाना जाता है लेकिन आज भी शहर में कोई अठारह लाख लीटर पानी प्रति दिन एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से वितरित होता है, जिसका निर्माण 1615 में किया गया था। यह प्रणाली जल संरक्षण और वितरण की दुनिया की अजूबी मिसाल है, जिसे ‘भंडाराÓ कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाडिय़ों से एक-एक बूंद जल जमा करना और उसे नहरों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाने की यह व्यवस्था मुगलकाल में फारसी जल-वैज्ञानिक तबकुतुल अर्ज ने तैयार की थी। समय की मार के चलते दो भंडारे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं।

सनद रहे कि हमारे पूर्वजों ने देश-काल-परिस्थिति के अनुसार बारिश को समेट कर रखने की कई पण्रालियां विकसित और संरक्षित की थीं, जिनमें तालाब सबसे लोकप्रिय थे। घरों की जरूरत यानी पेयजल और खाना बनाने के लिए मीठे पानी का साधन कुआं कभी हर घर-आंगन में हुआ करता था। धनवान सार्वजनिक कुएं बनवाते थे। हरियाणा से मालवा तक जोहड़ या खाल जमीन की नमी बरकरार रखने की प्राकृतिक संरचना हैं। ये आम तौर पर वष्रा-जल के बहाव क्षेत्र में पानी रोकने के प्राकृतिक या कृत्रिम बांध के साथ छोटे तालाब की मानिंद होते हैं। तेज ढलान पर तेज गति से पानी के बह जाने वाले भूस्थल में पानी की धारा को काट कर रोकने की पद्धति ‘पाटÓ पहाड़ी क्षेत्रों में लोकप्रिय रही है। एक नहर या नाली के जरिए किसी पक्के बांध तक पानी ले जाने की प्रणाली ‘नाड़ा या बंधाÓ अब देखने को नहीं मिल रही। कुंड और बावडिय़ा महज जल संरक्षण के साधन नहीं, बल्कि हमारी स्थापत्य कला के बेहतरीन नमूना रहे हैं। आज जरूरत है कि ऐसी पारंपरिक पण्रालियों को पुनर्जीवित करने के लिए खास योजना बनाई जाए और इसकी जिम्मेदारी स्थानीय समाज की ही हो।
यह देश-दुनिया जब से है तब से पानी अनिवार्य जरूरत रही है और अल्प वष्रा, मरुस्थल, जैसी विषमताएं प्रकृति में विद्यमान रही हैं-यह तो बीते दो सौ साल में ही हुआ कि लोग भूख या पानी के कारण अपने पुश्तैनी घरों-पिंडों से पलायन कर गए। उसके पहले का समाज तो हर तरह की जल-विपदा का हल रखता था। अभी हमारे देखते-देखते ही घरों के आंगन, गांव के पनघट और कस्बों के सार्वजनिक स्थानों से कुएं गायब हुए हैं। बावडिय़ों को हजम करने का काम भी आजादी के बाद ही हुआ। हमारा आदि-समाज गर्मी के चार महीनों के लिए पानी जमा करने और किफायत से खर्च करने को अपनी संस्कृति मानता था। अपने इलाके के मौसम, जलवायु चक्र, भूगर्भ, धरती-संरचना, पानी की मांग-आपूर्ति का गणित भी जानता था। उसे पता था कि खेत को कब पानी चाहिए और कितना मवेशी को और कितने में कंठ तर हो जाएगा। वह अपनी गाड़ी को साफ करने के लिए पाइप से पानी बहाने या हजामत के लिए चालीस लीटर पानी बहा देने वाली टोंटी का आदी नहीं था। भले ही आज उसे बीते जमाने की तकनीक कहा जाए लेकिन आज भी देश के कस्बे-शहर में बनने वाली जल योजनाओं में पानी की खपत और आवक का वह गणित कोई नहीं आंक पाता है, जो हमारा पुराना समाज जानता था।
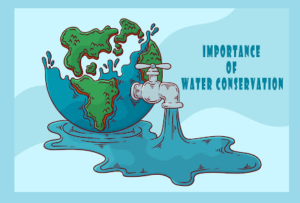
राजस्थान में तालाब, बावडिय़ां, कुई और झालार सदियों से सूखे का सामना करते रहे। ऐसे ही कर्नाटक में कैरे, तमिलनाडु में ऐरी, नगालैंड में जोबो तो लेह-लद्दाख में जिंग, महाराष्ट्र में पैट, उत्तराखंड में गुल, हिमाचल प्रदेश में कुल और जम्मू में कुहाल कुछ ऐसे पारंपरिक जल-संवर्धन के सलीके थे जो आधुनिकता की आंधी में कहीं गुम हो गए और आज जब पाताल का पानी निकालने और नदियों पर बांध बनाने की जुगत नाकाम होती दिख रही हैं तो फिर उनकी याद आ रही है। गुजरात में कच्छ के रण में पारंपरिक मालधारी लोग खारे पानी के ऊपर तैरती बारिश की बूंदों के मीठे पानी को ‘विरदाÓ के प्रयोग से संरक्षित करने की कला जानते थे। सनद रहे कि उस इलाके में बारिश भी बहुत कम होती है। हिम-रेगिस्तान कहे जाने वाले लेह-लद्दाख में सुबह बरफ रहती है, और दिन में धूप के कारण कुछ पानी बनता है जो शाम को बहता है। वहां के लोग जानते थे कि शाम को मिले पानी को सुबह कैसे इस्तेमाल किया जाए।
तमिलनाडु में एक जल सरिता या धारा को कई-कई तालाबों की श्रृंखला में मोड़कर हर बूंद को बड़ी नदी और वहां से समुद्र में बेजा होने से रोकने की अनूठी परंपरा थी। उत्तरी अराकोट और चेंगलपेट जिले में पलार एनीकेट के जरिए इस ‘पद्धति तालाबÓ प्रणाली में 317 तालाब जुड़े हैं। रामनाथपुरम में तालाबों की अंतश्र्रृंखला भी विस्मयकारी है। पानी के कारण पलायन के लिए बदनाम बुंदेलखंड में भी पहाड़ी के नीचे तालाब, पहाड़ी पर हरियाली वाला जंगल और एक तालाब के ‘ओनेÓ (अतिरिक्त जी की निकासी का मुंह) से नाली निकाल कर उसे उसके नीचे धरातल पर बने दूसरे तालाब से जोडऩे और ऐसे पांच-पांच तालाबों की कतार बनाने की परंपरा 900वीं सदी में चंदेल राजाओं के काल से रही है। वहां तालाबों के आंतरिक जुड़ावों को तोड़ा गया, तालाब के बंधान फोड़े गए, तालाबों पर कालोनी या खेत के लिए कब्जे हुए, पहाड़ी फोड़ी गई, पेड़ उजाड़ दिए गए। इसके कारण जब जल देवता रूठे तो पहले नल, फिर नलकूप के टोटके किए गए। सभी उपाय जब हताश रहे तो आज फिर तालाबों की याद आ रही है।
 The Blat Hindi News & Information Website
The Blat Hindi News & Information Website




